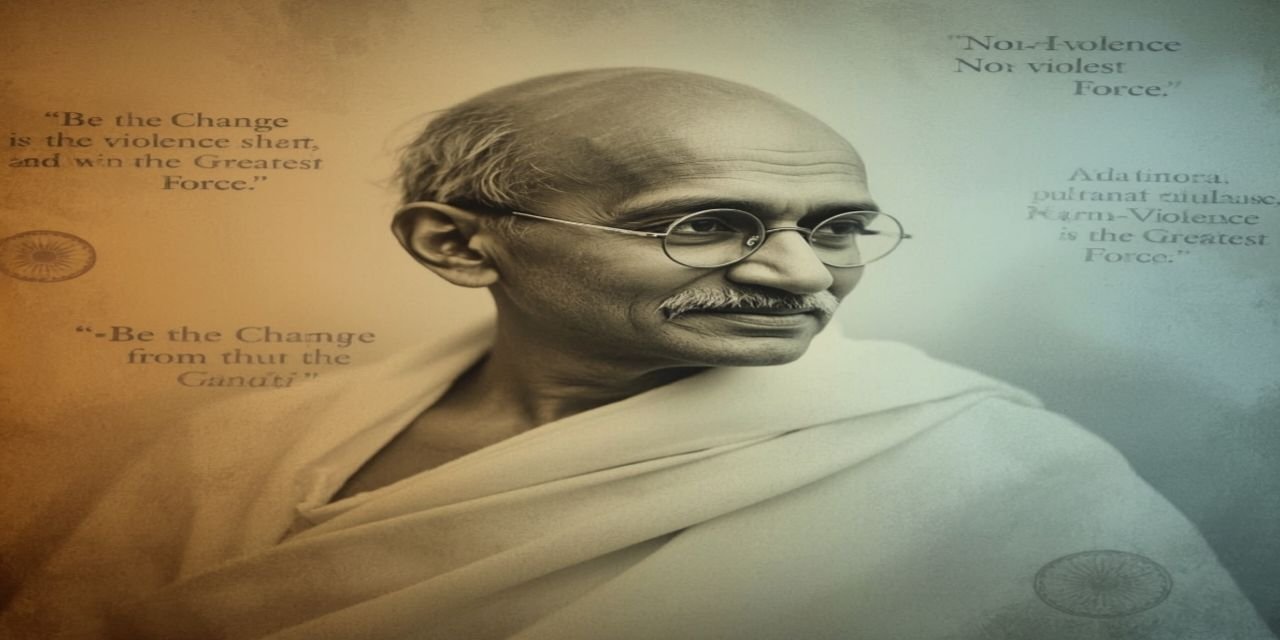Delhi History यानी दिल्ली का इतिहास, सत्ताओं के उत्थान और पतन की अद्वितीय गाथा है। इस गाथा में एक ऐसा अध्याय आता है जो अत्यंत संक्षिप्त, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है — Nasir-ud-Din खुसरू शाह की दो महीने की सल्तनत। 14वीं सदी की शुरुआत में जब खिलजी वंश का पतन हो रहा था, तब इस उथल-पुथल के दौर में खुसरू शाह ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यह वह समय था जब सत्ता के लिए राजनीतिक साजिशें, विश्वासघात और विश्वास की जटिलताएं चरम पर थीं।
खुसरू शाह का असली नाम हसन था और वे बारादस समुदाय से थे, जिन्हें खिलजी शासकों ने गुलाम बनाया था और फिर इस्लाम में धर्मांतरित कर उच्च पदों तक पहुंचाया। मुबारक शाह की हत्या के बाद उन्होंने खुद को Nasir-ud-Din की उपाधि दी और 1320 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बन गए। लेकिन उनका शासन केवल दो महीने चला, जो Delhi History के सबसे छोटे और विवादास्पद शासनों में गिना जाता है।
दिल्ली की राजधानी होने के नाते यहां सत्ता का हर परिवर्तन पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करता था। खुसरू शाह के शासनकाल में पारंपरिक तुर्क-अफगान अमीरों और धर्मगुरुओं ने एक धर्मांतरित गुलाम के राजा बनने पर विरोध जताया। उन्होंने अपने भरोसेमंद बारादस अनुयायियों को प्रशासनिक पदों पर बैठाया, जिससे पूरे तंत्र में असंतुलन आ गया। Delhi History के दृष्टिकोण से यह दौर एक अस्थायी राजनीतिक प्रयोग की तरह रहा, जहाँ वैधता की बजाय शक्ति और साजिश हावी थे।
जल्द ही गाजी मलिक तुगलक ने इस अस्थायी शासन को समाप्त कर दिया और तुगलक वंश की नींव रखी। लेकिन Nasir-ud-Din खुसरू शाह का यह अल्पकालीन शासन यह दर्शाता है कि दिल्ली की सत्ता केवल तलवार और रणनीति से नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ी होती है।
Delhi History में Nasir-ud-Din खुसरू शाह का शासन एक ऐसा पड़ाव है, जो सत्ता के अस्थायित्व और सामंतवादी विद्रोहों की स्पष्ट झलक देता है — यह अध्याय भले ही छोटा हो, पर इसकी गूंज इतिहास में गहरी है।
जौना का दिल्ली से साहसी पलायन: खुसरू शासन के अंत की शुरुआत

1320 ईस्वी में जब Nasir-ud-Din खुसरू शाह की दो महीने की सल्तनत अपने चरम पर थी, तब दिल्ली दरबार के भीतर असंतोष की आग भी धीरे-धीरे धधक रही थी। दिल्ली में खुसरू शाह के बारादस अनुयायियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, और यह स्थिति कई पुराने तुर्क अमीरों के लिए अपमानजनक थी। इन्हीं में से एक थे फखर-उद-दीन जौना, जिन्हें इतिहास में आगे चलकर मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। वह उस समय दिल्ली के शाही अस्तबल के प्रभारी थे और उन्होंने बारादस के बढ़ते प्रभुत्व से निराश होकर अपने पिता गाजी मलिक तुगलक से संपर्क साधने की ठानी।
जौना ने एक गुप्त बैठक बुलाई जिसमें उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गाजी मलिक तुगलक को एक विस्तारपूर्ण संदेश भेजा जाए जिसमें दिल्ली की ताजा स्थिति, खुसरू शाह की नीतियों और बारादस के अत्यधिक हस्तक्षेप का उल्लेख हो। यह संदेश अली याघदी नामक एक विश्वसनीय दूत के माध्यम से दीपलपुर भेजा गया। जवाब में, गाजी मलिक ने अपने पुत्र को तुरंत दिल्ली छोड़ने और उनसे आकर मिलने का आदेश दिया।
इब्न बत्तूता के विवरण के अनुसार, जौना ने खुसरू से कहा कि उनके घोड़े अधिक वजन उठा रहे हैं और उन्हें थोड़ा व्यायाम करना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने रहें। खुसरू, जो उस समय जौना पर संदेह नहीं कर रहा था, ने उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद जौना हर दिन कुछ घंटों के लिए बाहर जाने लगे। यह योजना का हिस्सा था। धीरे-धीरे उन्होंने शाही अस्तबल से सबसे बेहतरीन घोड़ों का चयन कर लिया।
अंततः एक दिन, जौना अपने वफादार अनुयायियों, बहरम अबिया के बेटे और अन्य भरोसेमंद सैनिकों के साथ, सूर्यास्त से पहले निकल पड़े और दीपलपुर की दिशा में एक साहसी पलायन को अंजाम दिया। यह घटना केवल व्यक्तिगत विद्रोह नहीं थी, बल्कि खुसरू शाह के शासन के अंत की शुरुआत थी। जौना का यह साहसिक कदम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया जिसने तुगलक वंश के उदय और दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।
यह पलायन, जो एक कूटनीतिक चाल और रणनीतिक योजना का हिस्सा था, दिल्ली के इतिहास में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ।
खुसरू शाह की प्रतिक्रिया और तुगलक की निर्णायक तैयारी: युद्ध की पूर्वपीठिका

जैसे ही जौना (भविष्य के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक) के दिल्ली से भागने की खबर खुसरू शाह के दरबार तक पहुँची, उसने अपनी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खो दी। सत्ता में बने रहने के लिए पहले ही संघर्ष कर रहे खुसरू को यह पलायन एक व्यक्तिगत विश्वासघात और रणनीतिक चुनौती की तरह लगा। Delhi History में यह वह क्षण है जब खुसरू शाह का डर, उसकी आक्रामकता में बदल गया। उसने तत्काल अपने दरबारियों और सलाहकारों की बैठक बुलाई, लेकिन डर और भ्रम की स्थिति में एक भयानक फैसला ले लिया।
अलाउद्दीन खिलजी के तीन अंधे पुत्र – अली, बहर और उस्मान – जिन्हें वर्षों से शाही महल में लाल वस्त्र पहनाकर कैदियों की तरह रखा गया था, को खुसरू शाह ने बेरहमी से मार डालने का आदेश दिया। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे खिलजी वंश के वंशज थे, और जनता व अमीरों के लिए एक वैकल्पिक नेतृत्व की संभावना बन सकते थे। यह घटना न केवल एक नैतिक विफलता थी, बल्कि एक रणनीतिक भूल भी, जिसने खुसरू के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया।
खुसरू ने सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अमीरों और रईसों को धन के लालच से खरीदने की कोशिश की। सोने-चांदी की थैलियाँ दरबारियों में बाँटी गईं ताकि उनकी वफादारी खरीदी जा सके, लेकिन दिल्ली जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील शहर में यह उपाय अल्पकालिक ही साबित हुआ। जौना को पकड़ने के लिए खुसरू ने शिस्ता खान की अगुआई में एक सैन्य अभियान चलाया, लेकिन वे सरसुति तक पहुँचे बिना ही असफल होकर लौट आए। दरअसल, जौना पहले से ही दीपलपुर पहुँच चुके थे और उनके पिता तुगलक ने वहां के किले की सुरक्षा को सुदृढ़ कर दिया था।
आरंभ में खुसरू ने तुगलक से संधि करने की कोशिश की। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि तुगलक को उनके राज्य की स्वायत्तता दी जाएगी, साथ ही उनके क्षेत्र का विस्तार भी संभव होगा। लेकिन सूफी खान जैसे सलाहकारों ने खुसरू को आगाह किया कि यदि तुगलक को खुली छूट दी गई, तो वह एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसके जवाब में एक दूत को तुगलक के पास भेजा गया, जो खुसरू की सर्वोच्चता को स्वीकार करने का संदेश लेकर गया था।
तुगलक ने इस दूत को मार डाला, और एक अवमानना और आक्रोश से भरा पत्र खुसरू को भेजा। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अब सुलह की कोई संभावना नहीं बची थी। इसके बाद तुगलक और उनके पुत्र जौना ने पूरी तैयारी के साथ युद्ध का निर्णय लिया। तुगलक ने उत्तर भारत के प्रमुख प्रांतों और शासकों को पत्र भेजे – जिनमें बहरम अबिया (उच के गवर्नर), मुगलती (मुल्तान के गवर्नर), मुहम्मद शाह (सिविस्तन के गवर्नर), याकलाखी (समाना के गवर्नर), होशांग (जेलोर के गवर्नर), और ऐन-उल-मुल्क मुलनी शामिल थे।
तुगलक ने अपने इस संघर्ष को इस्लाम की रक्षा, खिलजी वंश के प्रति वफादारी, और दिल्ली में अपराधियों को दंडित करने का नैतिक दायित्व घोषित किया। यह सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि एक वैचारिक युद्ध बन चुका था — एक ऐसा युद्ध जिसने अंततः Nasir-ud-Din खुसरू शाह के शासन का अंत कर दिया और दिल्ली की बागडोर तुगलक वंश के हाथों में सौंप दी।
Delhi History का निर्णायक मोड़: तुगलक की बढ़ती ताकत और Nasir-ud-Din खुसरू शाह की घबराहट
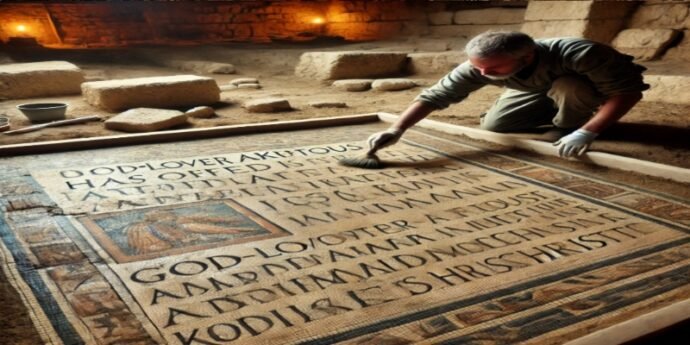
जब दिल्ली की सत्ता को लेकर संघर्ष अपने चरम पर था, तब तुगलक ने एक चतुर रणनीति के तहत Delhi History को एक नई दिशा देने के लिए उत्तर भारत के प्रमुख सूबेदारों और अमीरों से संपर्क साधा। उसका उद्देश्य सिर्फ सैन्य बल एकत्र करना नहीं था, बल्कि राजनीतिक समर्थन और वैधता भी अर्जित करना था। इस पहल का सबसे सकारात्मक परिणाम बहरम अबिया के रूप में सामने आया, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुगलक का समर्थन किया और अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ तुगलक से आ मिले।
मगर हर शासक इतना सीधा नहीं था। मुगलती, मुल्तान के अमीर, ने तुगलक को समर्थन तो दिया, लेकिन खुले विद्रोह से इंकार कर दिया। उन्होंने अपनी सीमित घुड़सवार और पैदल सेना का हवाला देते हुए दिल्ली के खिलाफ विद्रोह करने की असमर्थता जताई। यह जवाब तुगलक को स्वीकार्य नहीं था। उसने कूटनीति और षड्यंत्र के सहारे मुल्तान के अन्य अमीरों को मुगलती के खिलाफ भड़काया। इसका नतीजा हुआ – एक सफल विद्रोह। बहरम सिरज के नेतृत्व में विद्रोह भड़का, और मुगलती को मुल्तान से भागना पड़ा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका – उसे पकड़ लिया गया और उसका सिर कलम कर दिया गया। यह घटना तुगलक की राजनीतिक चतुराई का प्रमाण थी।
वहीं दूसरी ओर, याकलाखी, जिसने पहले Nasir-ud-Din खुसरू शाह के आदेश पर अपने कान और नाक खो दिए थे, फिर भी खुसरू के प्रति वफादार बना रहा। तुगलक का पत्र उसके पास पहुंचा तो उसने उसे खुसरू को दिखा दिया, जिससे खुसरू को आने वाले विद्रोह की खबर मिल गई। जवाब में याकलाखी ने दीपलपुर पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन तुगलक की तैयार सेना ने उन्हें हरा दिया। याकलाखी भागकर समाना पहुँचा, जहाँ उसे अपने ही लोगों द्वारा मार डाला गया — यह उस राजनीतिक उथल-पुथल की गवाही थी जो उस समय की Delhi History का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी।
मुहम्मद शाह, सिविस्टन के गवर्नर, उस समय अपने ही रईसों द्वारा बंदी बना लिए गए थे। लेकिन जब उन्हें तुगलक का संदेश मिला, तब उनके रईसों ने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह तुगलक की सेना में शामिल होने के लिए सहमत हों, तो उन्हें रिहा किया जाएगा। मुहम्मद शाह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तुगलक से जा मिले। इसके साथ ही होशांग, जेलोर के गवर्नर, ने भी तुगलक को समर्थन दिया। हालांकि, दोनों गवर्नर तब तक दिल्ली नहीं पहुँच सके जब तक तुगलक ने वहां तख्त पर कब्जा नहीं कर लिया।
ऐन-उल-मुल्क मुल्तानी का रवैया पूरी तरह तटस्थ था। उसने तुगलक का पत्र Nasir-ud-Din खुसरू शाह को दिखाया, जिससे खुसरू को तुगलक की बढ़ती पकड़ का एहसास हुआ। तुगलक ने उसे अपने पक्ष में लाने के लिए एक दूत भेजा, लेकिन मुल्तानी ने जवाब में कहा कि वह किसी पक्ष का समर्थन नहीं करेगा। उसने संकेत दिया कि वह उसी का साथ देगा जो दिल्ली की घेराबंदी करेगा – यानी जो विजेता होगा, उसे ही उसकी निष्ठा मिलेगी।
इस बीच, तुगलक की शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही थी। बहरम अबिया के समर्थन के साथ-साथ अब खोकर्स, जो एक शक्तिशाली योद्धा जाति थे, भी तुगलक से आ मिले। इन नए समर्थनों ने तुगलक की सेना को मजबूत किया और उसकी राजनीतिक साख को भी बढ़ाया। इसी दौरान तुगलक के अधिकारियों ने एक कारवां को रोका जो मुल्तान और सिविस्टन से दिल्ली की ओर शाही राजस्व और घोड़ों को ले जा रहा था। तुगलक ने इस लूट का इस्तेमाल अपनी सेना को हथियारों और घोड़ों से लैस करने में किया। अब वह पूरी तरह से तैयार था।
दीपलपुर से Delhi की ओर बढ़ते हुए तुगलक ने हर मोर्चे पर योजना बनाई। दूसरी ओर, Nasir-ud-Din खुसरू शाह, जो अब तक अपनी सेना की शक्ति और राजधानी की सुरक्षा पर भरोसा कर रहा था, धीरे-धीरे घबराने लगा। तुगलक की हरकतें उसके लिए स्पष्ट संकेत थीं कि युद्ध अब दूर नहीं है।
इस स्थिति को भांपते हुए, खुसरू शाह ने अपने भाई, खान-ए-खानन के नेतृत्व में एक विशाल सेना को तुगलक का सामना करने के लिए भेजा। यह टकराव अब केवल सत्ता के लिए नहीं था – यह Delhi History की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक बनने जा रहा था, जो एक शासक के पतन और एक नए वंश के उदय की पटकथा लिखने वाला था।
खुसरू खान की निर्णायक हार: Delhi History में सत्ता परिवर्तन का युगांतकारी क्षण

1320 ईस्वी की वह सुबह Delhi History में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब दो सेनाएं आमने-सामने खड़ी थीं — एक तरफ Nasir-ud-Din खुसरू शाह की सेना, जो अपने पतन की कगार पर थी, और दूसरी तरफ गाजी मलिक तुगलक की सेना, जो नई सल्तनत की नींव रखने को तैयार थी। यह टकराव सरसुति के पास हौज़-ए-नाहत पर हुआ, जो दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर स्थित तुगलक की रक्षा चौकी थी।
खुसरू शाह ने अपने भाई खान-ए-खानन को कमान सौंपते हुए अपने दल को चार भागों में बाँटा। उसने खुद को सेनानायक के रूप में केंद्र में तैनात किया और उसके पास परसोल (राजसी छत्र) उठाया गया, जो नेतृत्व और सत्ता का प्रतीक था। कुतला ने अग्रिम मोर्चे की जिम्मेदारी ली, तलबागा याघदा ने बाएँ हिस्से की कमान संभाली, और दाहिनी ओर नाग, काचिप, वर्मा तथा अन्य बारादस सैनिक तैनात किए गए।
तुगलक की योजना उससे कहीं अधिक व्यवस्थित थी। खुद तुगलक सेना के केंद्र में खड़ा था, जबकि उसका पुत्र जौना (मुहम्मद बिन तुगलक) उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके साथ थे खोकर योद्धा, जिनमें गुलाबी चंद और साहज राय प्रमुख थे। बाईं ओर बहराम अबिया खड़े थे और दाहिनी ओर तुगलक के भतीजे असद-उद-दीन और बहा-उद-दीन गरशास्प ने मोर्चा संभाला।
जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, खोकर योद्धाओं ने कुतला के मोर्चे पर भयंकर हमला बोला। यह हमला इतनी तीव्रता से किया गया कि कुतला अपने घोड़े से गिर पड़ा और मारा गया। उसकी टुकड़ी पूरी तरह से बिखर गई और वे सभी केंद्र की ओर भाग निकले। यह Nasir-ud-Din खुसरू शाह की सेना के लिए एक गंभीर झटका था। इससे पहले कि वे स्थिति संभाल पाते, तुगलक की सेना ने पूरी ताकत के साथ केंद्र पर धावा बोल दिया।
खान-ए-खानन, जो कभी भी किसी बड़ी सेना का नेतृत्व नहीं कर चुका था, घबरा गया। उसने अपने साथियों — यूसुफ सूफी खान, शिस्ता खान और काद्र खान — के साथ युद्धस्थल से भागने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसकी सेना के मनोबल को और गिरा गया।
उसी दौरान, खोकर प्रमुख गुला ने खुसरू की सेना के छाता वाहक को मार गिराया और उसका छत्र छीन लिया। यह छत्र तुगलक की सेना के लिए न केवल एक प्रतीकात्मक विजय थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी। जब यह छत्र तुगलक के सिर पर उठाया गया, तो युद्ध के नतीजे स्पष्ट हो गए — यह केवल एक विजय नहीं थी, यह सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा थी।
इस निर्णायक जीत के बाद, गाजी मलिक तुगलक ने अपनी विजयी सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। राजधानी के बाहरी क्षेत्र में स्थित सुल्ताना रज़िया की कब्र के परिसर में उन्होंने अपने शिविर की स्थापना की। यहाँ से उन्होंने रणनीतिक रूप से अपनी सेनाओं की पुनः स्थिति निर्धारित की और अगले कदम की योजना बनाई।
यह लड़ाई केवल दो सेनाओं के बीच नहीं थी। यह Delhi History में उस समय की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों का प्रतिबिंब थी। एक ओर खुसरू शाह था, जो जातीय रूप से बारादस था और हाल ही में मुसलमान बना था। उसका शासन दो महीने तक चला, जिसमें उसने अनेक विवादास्पद फैसले लिए और कई अमीरों को नाराज किया। दूसरी ओर, गाजी मलिक तुगलक था — एक कुशल रणनीतिकार, अनुभवी सेनापति और इस्लाम की पारंपरिक रक्षा के नाम पर युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति।
Nasir-ud-Din खुसरू शाह की हार इस बात का प्रमाण थी कि सत्ता केवल छल और षड्यंत्र से नहीं टिकती। वैधता, सामरिक कौशल, और जनता तथा अमीरों का समर्थन आवश्यक था — और इन तीनों में खुसरू पिछड़ चुका था। यही कारण है कि उसकी दो महीने की सल्तनत Delhi History की सबसे संक्षिप्त लेकिन शिक्षाप्रद सल्तनतों में से एक मानी जाती है।
अंततः, इस निर्णायक टकराव ने न केवल एक शासक का अंत किया, बल्कि दिल्ली में एक नए युग की शुरुआत की — तुगलक वंश का, जिसने आगे चलकर मध्यकालीन भारत की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल दिया।